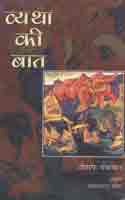|
लेख-निबंध >> व्यथा की बात व्यथा की बातजोसफ मॅकवान
|
403 पाठक हैं |
||||||
श्रमजीवी और उपेक्षित समाज के महत् चरित्रों पर लेखन....
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
‘व्यथा की बात’ गुजराती भाषा के महान लेखक जोसफ
मॅकवान के चुने हुए गुजराती रेखाचित्रों का हिन्दी अनुवाद है। उपन्यास के
पाठ का आनंद देने वाला यह संकलन न केवल गुजरात जनपद के जीवन-यापन,
आचार-विचार, सुख-सुविधा, दुख-दुविधा की झांकी प्रस्तुत करता है बल्कि बड़े
फलक पर एक संवेदनशील रचनाकार की गहरी जीवन-दृष्टि का परिचय भी देता है।
संकलन के ज्यादातर निबंध आत्मकथा की तरह लिखे गए हैं। पर प्रभाव में ये
रचनाएं पूरे देश के आम जनमानस में फैले राग-द्वेष, जय-पराजय,
बुद्धि-विवेक, सत्-असत्, सुख-दुख के सूक्ष्म चित्र अंकित करती हैं और बड़ी
साफगोई से मानव मन की आंतरिक बुनावट को उजागर करती हैं।
इस पुस्तक के लेखक जोसफ मॅकवान (9.10.1936) ने गुजरात में दलित लेखक के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त की। बीसवीं शताब्दी के छठे दशक में इन्होंने लेखन कार्य प्रारंभ किया। श्रमजीवी और उपेक्षित समाज के महत् चरित्रों पर नजर रखना इनके रचनाधर्म का केन्द्रीय कार्य है। ‘आंगलियात’ उपन्यास के लिए इन्हें साहित्य अकादमी सम्मान (1989) मिला। गुजराती भाषा साहित्य में जोसफ मॅकवान का साहित्य महत्त्वपूर्ण और अगली पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्पद स्वर का काम करता है।
अनुवादक गोपालदास नागर एक प्रतिष्ठा प्राप्त अनुवादकर्मी और साहित्यधर्मी हैं। गुजराती से हिन्दी तथा हिन्दी से गुजराती में अनुवाद कर्म का श्रेष्ठ नमूना प्रस्तुत करने के अलावा साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र में और भी कई महत्त्वपूर्ण काम इन्होंने किए हैं।
इस पुस्तक के लेखक जोसफ मॅकवान (9.10.1936) ने गुजरात में दलित लेखक के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त की। बीसवीं शताब्दी के छठे दशक में इन्होंने लेखन कार्य प्रारंभ किया। श्रमजीवी और उपेक्षित समाज के महत् चरित्रों पर नजर रखना इनके रचनाधर्म का केन्द्रीय कार्य है। ‘आंगलियात’ उपन्यास के लिए इन्हें साहित्य अकादमी सम्मान (1989) मिला। गुजराती भाषा साहित्य में जोसफ मॅकवान का साहित्य महत्त्वपूर्ण और अगली पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्पद स्वर का काम करता है।
अनुवादक गोपालदास नागर एक प्रतिष्ठा प्राप्त अनुवादकर्मी और साहित्यधर्मी हैं। गुजराती से हिन्दी तथा हिन्दी से गुजराती में अनुवाद कर्म का श्रेष्ठ नमूना प्रस्तुत करने के अलावा साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र में और भी कई महत्त्वपूर्ण काम इन्होंने किए हैं।
भूमिका
श्री जोसफ मकवान (जन्म 09-10-1936, तणोली,
तालुका आणंद) ने दलित लेखक के रूप में गुजरात में प्रतिष्ठा प्राप्त की है। उपन्यास के
क्षेत्र में पुरस्कृत हुए, लोकप्रियता प्राप्त की। ‘व्यथा की बात’ (व्यथानां वीतक) में भी यह संभावना मौजूद है। श्रमजीवी और उपेक्षित समाज के महत् चरित्रों की पहचान-श्री जोसफ मकवान की मुख्य पूंजी है। यह पूंजी अनेक तरह से और अनेक रूप में कथा-साहित्य में फलित हुई है। जोसफ व्यवसाय से शिक्षक रहे हैं, लेकिन गांठ के पैसे से सामाजिक परिवर्तन के लिए लोक शिक्षा देने निकल पड़े। अपनी जन्मभूमि के विकास में वे सदा लगे रहे हैं। उन्होंने पत्रकारिता को भी दलितों के वकील के रूप में अपनाया। साठ वर्ष की आयु में भी लड़ने की, संघर्ष करने की खुमारी टिकी रही है। फिर भी कहना चाहिए कि वे पक्षधर की अपेक्षा सहिष्णु ही अधिक हैं। कैथोलिक ईसाई
की उदारता ने उन्हें दलित लेखक के रूप में भी टिका रखा है। वह पादरी बने
होते तो भी निभा ले गए होते। अच्छा हुआ कि वे लेखन से जुड़ गए। एक बार
किनारे आकर फिर वापस प्रवाह में खिंचे। वे सामाजिक पहले हैं, धार्मिक बाद
में।
जोसफ ने लेखन की शुरुआत छठे दशक में की थी। सन् 1956 से 1964 तक मुग्धभाव से लिखा। साहित्यिक प्रणालियों का पालन किया। पुरस्कार प्राप्त किए। आठवें दशक में अमृतराय आदि प्रगतिशील साहित्यकारों के प्रभाव में आए। शिविरों, संपर्कों का लाभ मिला। समाजसेवा और राजनीति की प्रवृत्तियां चालू थीं। भानु भाई अध्वर्यु और अन्य समाजलक्षी विचारकों के प्रभाव से तथा चंदु महेरिया जैसे मित्रों के आग्रह से जोसफ ने दूसरी बार कलम उठाई। इस बार क्या लिखना है, किस विषय पर लिखना है, किसलिए लिखना है-इन सबका पूरा ध्यान और स्पष्टता थी। दुर्गा भागवत को उद्धृत कर जोसफ कहते हैं-
‘‘हमारा आज का साहित्य साढ़े तीन टके (प्रतिशत) का साहित्य है। साढ़े तीन टका जन जीवन का प्रतिनिधित्व या साढ़े तीन टका उच्चजातियों के जमाए सामाजिक असरों का साहित्य, तो फिर बाकी के साढ़े छियानबे प्रतिशत लोगों का क्या?’’ साढ़े छियानबे प्रतिशत के बारे में बात करने का यह जोखिम लेखक समझते हैं। कहते हैं:
‘‘आप कवियों को, मुशायरा अच्छा लगता है और कवि सभा खुशी से आयोजित करते हैं, लेकिन आप जो वेदना गाने वाले हैं, उससे कितनों को रोएं खड़े होंगे ? ‘फूल लीघा-दीघानी रढ़’ पुस्तक में आपके दर्द को कौन कितना महत्व देगा ? आइवरी टावर में विराजमान होकर लिखने वालों ने संप्रति साहित्य को व्याख्यायित किया है !
हमारा मेल वहां कम बैठेगा। हमारी रचनाओं से हमारे अपने लोग भावमग्न हो उठेंगे, हमारे ही निर्लज्ज कलेजे में चर्चा उठे, हमारा सर्वथा प्रमादी आलस्य ऐंठे, हमारे लोग जागें-संसार जागे, रूढ़ शब्द-अर्थ कहावत-कहानी के बंधन तोड़े, अलग निशान बनाएं तभी यह संभव होगा।’’
इस दावे में किसी को अतिशयोक्ति लगे तो भी मैं कहूंगा कि इस स्थिति मैं इसकी जरूरत है। यह मात्र दलित साहित्य के हित में ही नहीं, समग्र साहित्य के हित में है। क्यों ? परंपरागत साहित्यिक कृति रचने की अपेक्षा दलित जीवन के विषय में अछूती भाषा में लिखकर बहुजन समाज में पहुंचाना सरल नहीं। फिर आपकी पुस्तकें खरीदने वाला वर्ग तो उन साढ़े तीन प्रतिशत में से ही आने वाला है न...। उसके आधार पर साढ़े छियानबे प्रतिशत में प्रसारित होने वाला है। जो बिलकुल गरीब है उसे तो अपनी सारी आय अपने भरण-पोषण के पीछे ही खर्च करनी पड़ती है। जोसफ के बचपन के सगे-संबंधी के पास जाकर मैं नहीं कह सकूंगा कि लीजिए यह ‘व्यथा की बात’ पुस्तक आधे दाम में खरीद कर पढ़िए। खरीदने की बात तो बाद में, पेट भरने के लिए होने वाले उद्यम के बाद पढ़ने का समय मिलेगा भी ? फिर भी परिस्थिति की वक्रता देखिए, दलित साहित्य के प्रारंभिक समर्थक और संवर्धक तो गैर-दलित होने वाले हैं। राजनीति में ऐसा काम होता है। वहां बंटवारा हो जाता है। दल लड़ते हैं। साहित्य में बंटवारा टिकता नहीं। ‘आक्रोश’ से शुरू हुई बात आनंद में समाप्त होती है। इसलिए कहना होगा कि जोसफ मकवान द्वारा रचित रेखाचित्र सभी सहृदयों की संपत्ति बनेंगे।
एक शताब्दी पहले या उससे भी पहले गुजरात के उत्पीड़ित, उपेक्षित, गांव के अंतिम छोर पर रहते लोगों ने ईसाई धर्म अपनाया था। इससे अस्पृश्यता का कलंक गया, वह एक महत्व की घटना घटी। थोड़ी शिक्षा भी शुरू हुई। इन दो बुनियादी सुधारों के बाद भी जोसफ मकवान के सगे-संबंधी दलित किसलिए रहे ?
जोसफ मकवान पक्के ईसाई हैं और उनकी यह धार्मिक हैसियत भी छिपी नहीं। वे जब गुजरात के समाज की बात करते हैं, तब धार्मिक प्रवृत्ति के हिस्से (टुकड़े) नहीं करते। सामाजिक परिवर्तन के लिए गैरसांप्रदायिक दृष्टि यहां बुनियादी शर्त है। धर्म और अध्यात्म, यह व्यक्ति की निजी उपासना का विषय है। सामाजिक कंकाल को आर्थिक शक्तियां सतत प्रभावित करती हैं। इसलिए धर्म को अलग रखकर परिस्थितिजन्य दबाव सर्जित करने पड़ेंगे। उसमें शब्द का भी यत्किंचित हिस्सा हो सकता है। इस संन्दर्भ में ‘व्यथा की बात’ का स्वागत होना चाहिए।
सन् 1989 में इन्हें उपन्यास ‘आंगलियात’ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें दलित पुरुषों का अन्याय के विरुद्ध प्रतिकार, प्रेमियों का संयम, वर्ग-संघर्ष और दूसरों के लिए कुछ करने की भावना दृश्यात्मक घटनाओं द्वारा व्यक्त हुई है। खेड़ा जिला के हरिजन-ईसाइयों की बोलचाल की भाषा को योग्य बनाकर जोसफ ने एक नई ताकत पैदा की है। इस अर्थ में वे पूर्व पीढ़ी के उसी विस्तार के ईश्वर पेटलीकर की तुलना में अधिक महत्त्वपूर्ण हैं। सो हरिजनों-दलितों के आर्थिक-जातीय शोषण के प्रति पेटलीकर द्वारा दिखाई सहानुभूति के वे ऋणी है। नौवें दशक का उपन्यास पेटलीकर के उत्तराधिकारी की राह देखता था। जोसफ को मिली प्रतिष्ठा हमारे साहित्य के इतिहास की आवश्यकता थी।
संभव है, कलावादी धीरे-धीरे जोसफ से विमुख होते जाएं। क्योंकि लोकप्रियता जिस सरलता की अपेक्षा रखती है, वह बहुतेरे कलाविदों को चुभती है।
शायद ‘व्यथा की बात’ जोसफ के सर्जक व्यक्तित्व का मुख्य तत्त्व है। एक परिचित सृष्टि उनकी अपनी आबोहवा के साथ इस पुस्तक द्वारा सुलभ होती है।
जोसफ के भाषा-प्रभुत्व की मुख्य पद्घति यहां चमत्कृति का अनुभव कराती है। ‘आंगलियात’ में इसी शक्ति का उदय है। ‘व्यथा की बात’ के रेखांचित्र उपन्यास पढ़ने का आनंद देने के साथ भावुक पाठक की सामाजिक संप्रज्ञता भी बढ़ाते हैं। प्रश्न उठता है-मैं जिस गुजरात में रहता हूं उसे कितना पहचानता हूं ?
‘व्यथा की बात’ की रचनाएं मात्र रेखाचित्र हैं या उनमें उपन्यास की कला भी है ? लेखक को क्या सिद्ध करना है ?
‘व्यथा की बात’ के रेखाचित्र साहित्य की श्रेणी में आते हैं, इसका मुख्य कारण रशियन कथा-लेखक की तरह जोसफ के अनुभवों की पूंजी है, उनके द्वारा व्यक्त हुई समूह चेतना है। यहां तक आते-आते वे साहित्य में प्रयुक्त होते जाते बोलचाल के शब्दों की ध्वनि से परिचित हो चुके थे। यह पुस्तक प्रकाशित हुई तब उन्होंने पचासवें में प्रवेश कर लिया था, इसलिए रंगदर्शिता को शांत हृदय से नाथने की प्रौढ़ता उनमें आ चुकी थी। संग्रह लेकिन समस्त रेखाचित्रों में से किसी को कमतर कहने की गुंजाइश नहीं है। संग्रह के जिसमें अनोखापन अधिक हो, वैसा एक रेखाचित्र है ‘हेझल पद्मणी’। यह रेखा-चित्र स्वातंत्र्योत्तर कहानियों के संपादन में भी समाविष्ट हो सकता है। संतति की तीव्र लालसा और लोक-संस्कृति की नैतिकता के दो भिन्न परिबल इस कृति में एक मनोघटना सृजित करते हैं। बाह्य परिस्थिति की प्रतीतिजनक वास्तविकता उसमें सहायक बनती है।
‘हेझल का पति’ रुड़ा हज्जाम’ बाहर से आकर पंचों की स्वीकृति से इस गांव का निवासी बनता है। मुख्यरूप से बुनकरों का। पंचायत के प्रमुख अंधे मेठा ने कहा, ‘‘चमार हमारी तरफ, लेकिन भंगी अलग, उन्हें नहीं छूना होगा।’’
रुड़ा को साल के बारह रुपए किराए पर मिलता है। नीम के नीचे बैठकर वह सबसे बातें करता है। लेखक ने पहले की तरह ‘दो बाघ मिल जाएं’ वैसी देह और लड़कों की नजर में ‘कादू मकराणी’ कहकर उसकी शरीर संपदा का वर्णन किया था उसी तरह उसकी हज्जाम के रूप में उसकी कला को स्वीकार किया है :
‘‘रुड़ा का हाथ जितना हल्का था उतना ही रेशम जैसा था। सिर पर फिरता होता तो नींद के झोंके आते, चेहरे पर घूमता होता तो संगमरमर-सा चिकना लगता। जूं-लीख से भरे बालों वाले लड़कों का सिर अपनी टांग और जांघ से दबाकर सिर मूंड़ देता।’’ तीसरे झण फिर गंजा, सफाचट और फिर दूसरे लड़के चिढ़ाते, ‘बोडी तकोडी माथामां जींगोडी, बावो बोलावे तुंतुं !’ एक उतनी ही देर रुड़ा बुरा दिखता, बाकी वह सबको खूब अच्छा लगता।
यह वर्णन कल्पना से नहीं हो सकता, सूक्ष्म निरीक्षण चाहिए, जो जोसफ, मकवान ने बचपन में अनायास किया है। पति का पात्र निरुपित कर, उसके सौम्य लेकिन विषय व्यक्तित्व का निर्देश कर लेखक उसकी पत्नी का परिचय कराता है, ‘‘एक भरी दोपहरी में वह वापस आया तो हाथ भर का घूंघट निकाले एक नाजुक स्त्री, सेर-सेर भर के पायल झनकारती उसके पीछे चल रही थी। उसी शाम पंचों के आगे उस स्त्री ने आंचल फैलाया और सवा रुपए से उसकी गोद भरकर गांववालों ने नाई की पत्नी को अपना लिया। परछन करने वाली स्त्रियों ने बताया कि रुड़ा की पत्नी है तो रूप का टुकड़ा। हाल ही में स्वांग दिखाने वाले ‘होथल पद्मणि’ का नाटक दिखा गए थे। होथल गांव के लोगों की जबान पर चढ़ गई और अपने सुंदर रूप के कारण हेझल पद्मणि बन गई।’’
रुड़ा और हेझल का संसार अब दो परिप्रेक्ष्य में निरूपित होता है। हेझल के रूप में प्रभावित हुए लोगों के व्यवहार का आकर्षक शैली में आलेखन होता है तो स्वमानी और शीतवंती हेझल पति के पुत्र न होने की पीड़ा व्यक्त करती रहती है। एक बार उसकी बेसब्री बढ़ जाती है।
‘ऊपरवाला सब अच्छा करेगा।’ पति का यह अश्वासन भी उसे धैर्य नहीं बंधा पाता तब रुड़ा उसकी विशेषता के संबंध में एक बात कहता है। जैसे उसके विवाह गीतों की प्रशंसा होती, उसी तरह उसके कंठ से गाए जाते मरसिया (शोक गीत) से एक शोकाकुल वातावरण सृजित होता। लेकिन रुड़ा कहता है, ‘‘तुम्हारे गले से आवाज निकलती है और मेरे अंग गलने-पिघलने लगते हैं।...भले जो हो आकाश भी फटे, तो भी तुम्हें मरसिया तो नहीं ही गाना है। तुम्हारी मां....’’
हेझल की मां ने मारमल्ल दादा के सात मरसिया माने थे। वह जीते जी उसमें से पांच पूरे कर चुकी थी। बाकी रहे दो हेझल को गाने थे। मां की मृत्यु के समय की बात वह नहीं तोड़े। काफी गानेवालियों का सौभाग्य रहा है और घर-घर झूले (बच्चों के) बंधे हैं।
और रुड़ा गुस्से से जूता मारता है। कलाई उतर जाती है। सौभाग्य की सूचक चूड़ियों की जोड़ टूट जाती है...उस दिन उसने पति की बात का उल्लंघन करने का निश्चय किया था...लेकिन वह दूसरे गांव गया था तब हेझल की सहेली रतन के जवान पति की मृत्यु हो जाती है। बाहर से आई मरसिया गाने वाली ‘रुदाली’ नहीं है। इसलिए हेझल को बुलाया जाता है। पति की अरुचि हेझल को याद है। वह मना करती है। बात वहीं पूरी नहीं होती। पंचों की तरफ से अंधे मेठा का हुक्म होता है, ‘‘या तो गाओ या गांव, शहर और यह परगना छोड़कर जहां चाहो, चली जाओ।’’
यहां चलचित्र ‘रुदाली’ का स्मरण होता है। दूसरों की तरफ से शोक-गीत गाना, यही उनकी जीविका का आधार होता है।
कितने की विवेचक दलित साहित्य को सपाट और प्रचारात्मक कहकर उसकी निंदा करते हैं। यहां लौकिक वास्तविकता के साथ आधिभौतिक परिबलों, उन परिबलों के विषय में रुढ़ मान्यताओं, वृत्तियों और फिर उन्हें बदलने की वृत्ति-इन सबका कैसा संकुल आलेखन हुआ है !
रतन पंचों के आगे आंचल फैलाकर हेझल को गांव छोड़ने से बचाने का प्रयत्न करती, उससे पहले ही हेझल मरसिया गाने लगती है।
लेखक ने मरसिया तथा झंपताल के साथ पूरा होता मरसिया भी प्रस्तुत किया है। लेखक को इसकी मात्र जानकारी ही नहीं, वह स्वयं इससे वाकिफ भी है।
रतन की चूड़ियां तोड़ते-तोड़ते ही हेझल को मूर्छा आ जाती है।
पहले पति के साथ सम्मत न हुई हेझल अब ऐसी ग्रंथि से पीड़ित है कि पति की बात का उल्लंघन करने का पाप उसके लिए रुकावट बन गया। मां बनने के उसके अरमान अधूरे रह गए।
रतन डाक्टर की बात करती है। रुड़ा नकारता नहीं है, लेकिन डाक्टर के यहां साथ जाने के लिए राजी नहीं होता। हेझल के अंतिम मरसिया गाने के बाद से दोनों के बीच जैसे अंतर बढ़ जाता है। रतन के साथ हेझल अस्पताल जाती है, तब जवान डाक्टर हेझल को देखकर जैसे विस्मित-सा रह जाता है। स्वस्थ काया और तीन दशक का निखरा रूप ! ‘यही है हेझल ! कुछ समय पहले जिसने मरसिया गाया था ? डाक्टर उसका दर्द भूलकर उसकी देह को ही जैसे पढ़ने लगा था।’
दलित नारी के दर्द के इलाज के बहाने उसका जातीय शोषण कैसी चतुरता से होता है, इसका आलेखन बाद में हुआ है। कुछ मुलाकातों के बाद डाक्टर, हेझल के साथ छूट पा लेता है। हेझल जैसे सर्वस्व खो देती है। ‘ओरिजनल सीन’ की ईसाई ग्रंथि और भारत के ग्रामीण श्रमजीवी की नैतिक समानता यहां समझदारीपूर्वक हेझल के व्यवहार में व्यक्त होती है। रतन उसे समझाने का प्रयत्न करती तो वह कहती है, ‘‘मेरा भाग्य खराब, मेरा पेट कुपात्र, मेरा गला कुपात्र और मेरा जीवन भी कुपात्र। जीने की कोई इच्छा अब नहीं रही मुझे !’’
हेझल सूखती जाती है और एक सुबह कहीं चली जाती है। ढूंढ़ने गया रुड़ा एक महीने बाद वापस आता है। वह भले ही कहता है कि ‘हेझल मायके में है’, लेकिन उसकी ढीली आवाज हेझल के जिंदा होने का विश्वास नहीं दिलाती।
कथा के प्रारंभ का रुड़ा और हेझल कैसे-कैसे स्थित्यंतरों से गुजर कर कहां से कहां पहुंचते हैं। जिन परिबलों के कारण जहां उन्हें झेलने की स्थिति आती है, वहीं वाचाल बनकर ध्यान खींचना नहीं आता। लेकिन कृति का पहला वाक्य ‘दो बाध जितनी देह’ रुड़ा और हेझल दोनों के संदर्भ में अर्थ समर्पक फैसला है। अंत में जो संवेदना जागती है, वही मरसिया का धुंधला रुप धारण कर लेती है। हेझल चली गई है, उस दिशा में से कोई अरूप रुपाली गा रही है।
दलित समाज के दुख इतने अधिक हैं कि उनका यथावत् प्रतिबिंब शब्दस्थ किया जाए तो भी उसमें अतिशयोक्ति लगेगी। कभी कथा साहित्य की घटनाओं की अपेक्षा हकीकत, अधिक आश्चर्यजनक लगती हो, ऐसा लगता है। ‘घर का दीया’ में मेलोड्रामा-अतिरंजन का तत्व लगता है। लेकिन लेखक को तो तथ्य ही पेश करना था। सास विधवा हो और बहू भी विधवा हो जाए यह परिस्थिति एक दलित परिवार के लिए दुखों के हिसाब की अपेक्षा दुखों के गुणाकार जैसी है। पुत्र मरा तब बहू सगर्भा थी। बेटे को साथ लेकर मजदूरी पर जाती बहू, चेतन उड़ जाने के बाद भी मजदूरी करना चालू रखती है और मजदूरी का रुपया मिलने पर घर आती है। पहले वह रुपया आशी मां (सास) के हाथ में देती है और फिर ? ‘और यह आपके घर का दीया !’ मां और दादी मां के रुदन को अव्यक्त रखकर लेखक ने घुटन का अद्भुत अनुभव कराया है। मृत्यु यहां कैसे विविध रूप में आती है ! जिसने बारह वर्ष से बनवास लिया है उस ‘भवान भगत’ का जवानजोध लड़का मर गया है, यह समाचार सुनकर भवान भगत आकाश की तरफ नजर डालकर कहते हैं, ‘‘तुम मुझे चैन से मरने दोगे, ऐसा नहीं लगता !’’ जीवन भर की श्रद्धा विचलित कर देने वाली समझदार-से-समझदार आदमी को भी मूढ़ बना देने वाली मृत्यु ‘व्यथा की बात’ को मितभाषी बनाती है। हृदय-विदारक रुदन के सामने बाधक मौन उत्पन्न कर जोसफ मकवान ने सूक्ष्म कलासूत्र दर्शाया है।
यह पुस्तक गुजराती साहित्य के विद्यार्थियों ने पाठ्यपुस्तक के रूप में पढ़ी है। नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा भारत की विभिन्न भाषाओं में अनुवाद के लिए इसका चुनाव पाठकों को साहित्य का आस्वाद कराने के साथ ग्रामीण भारत के विशाल उपेक्षित श्रमजीवी वर्ग की पहचान भी देगी। यह पहचान परिवर्तन का इष्ट संकेत बन सकेगा।
जोसफ ने लेखन की शुरुआत छठे दशक में की थी। सन् 1956 से 1964 तक मुग्धभाव से लिखा। साहित्यिक प्रणालियों का पालन किया। पुरस्कार प्राप्त किए। आठवें दशक में अमृतराय आदि प्रगतिशील साहित्यकारों के प्रभाव में आए। शिविरों, संपर्कों का लाभ मिला। समाजसेवा और राजनीति की प्रवृत्तियां चालू थीं। भानु भाई अध्वर्यु और अन्य समाजलक्षी विचारकों के प्रभाव से तथा चंदु महेरिया जैसे मित्रों के आग्रह से जोसफ ने दूसरी बार कलम उठाई। इस बार क्या लिखना है, किस विषय पर लिखना है, किसलिए लिखना है-इन सबका पूरा ध्यान और स्पष्टता थी। दुर्गा भागवत को उद्धृत कर जोसफ कहते हैं-
‘‘हमारा आज का साहित्य साढ़े तीन टके (प्रतिशत) का साहित्य है। साढ़े तीन टका जन जीवन का प्रतिनिधित्व या साढ़े तीन टका उच्चजातियों के जमाए सामाजिक असरों का साहित्य, तो फिर बाकी के साढ़े छियानबे प्रतिशत लोगों का क्या?’’ साढ़े छियानबे प्रतिशत के बारे में बात करने का यह जोखिम लेखक समझते हैं। कहते हैं:
‘‘आप कवियों को, मुशायरा अच्छा लगता है और कवि सभा खुशी से आयोजित करते हैं, लेकिन आप जो वेदना गाने वाले हैं, उससे कितनों को रोएं खड़े होंगे ? ‘फूल लीघा-दीघानी रढ़’ पुस्तक में आपके दर्द को कौन कितना महत्व देगा ? आइवरी टावर में विराजमान होकर लिखने वालों ने संप्रति साहित्य को व्याख्यायित किया है !
हमारा मेल वहां कम बैठेगा। हमारी रचनाओं से हमारे अपने लोग भावमग्न हो उठेंगे, हमारे ही निर्लज्ज कलेजे में चर्चा उठे, हमारा सर्वथा प्रमादी आलस्य ऐंठे, हमारे लोग जागें-संसार जागे, रूढ़ शब्द-अर्थ कहावत-कहानी के बंधन तोड़े, अलग निशान बनाएं तभी यह संभव होगा।’’
इस दावे में किसी को अतिशयोक्ति लगे तो भी मैं कहूंगा कि इस स्थिति मैं इसकी जरूरत है। यह मात्र दलित साहित्य के हित में ही नहीं, समग्र साहित्य के हित में है। क्यों ? परंपरागत साहित्यिक कृति रचने की अपेक्षा दलित जीवन के विषय में अछूती भाषा में लिखकर बहुजन समाज में पहुंचाना सरल नहीं। फिर आपकी पुस्तकें खरीदने वाला वर्ग तो उन साढ़े तीन प्रतिशत में से ही आने वाला है न...। उसके आधार पर साढ़े छियानबे प्रतिशत में प्रसारित होने वाला है। जो बिलकुल गरीब है उसे तो अपनी सारी आय अपने भरण-पोषण के पीछे ही खर्च करनी पड़ती है। जोसफ के बचपन के सगे-संबंधी के पास जाकर मैं नहीं कह सकूंगा कि लीजिए यह ‘व्यथा की बात’ पुस्तक आधे दाम में खरीद कर पढ़िए। खरीदने की बात तो बाद में, पेट भरने के लिए होने वाले उद्यम के बाद पढ़ने का समय मिलेगा भी ? फिर भी परिस्थिति की वक्रता देखिए, दलित साहित्य के प्रारंभिक समर्थक और संवर्धक तो गैर-दलित होने वाले हैं। राजनीति में ऐसा काम होता है। वहां बंटवारा हो जाता है। दल लड़ते हैं। साहित्य में बंटवारा टिकता नहीं। ‘आक्रोश’ से शुरू हुई बात आनंद में समाप्त होती है। इसलिए कहना होगा कि जोसफ मकवान द्वारा रचित रेखाचित्र सभी सहृदयों की संपत्ति बनेंगे।
एक शताब्दी पहले या उससे भी पहले गुजरात के उत्पीड़ित, उपेक्षित, गांव के अंतिम छोर पर रहते लोगों ने ईसाई धर्म अपनाया था। इससे अस्पृश्यता का कलंक गया, वह एक महत्व की घटना घटी। थोड़ी शिक्षा भी शुरू हुई। इन दो बुनियादी सुधारों के बाद भी जोसफ मकवान के सगे-संबंधी दलित किसलिए रहे ?
जोसफ मकवान पक्के ईसाई हैं और उनकी यह धार्मिक हैसियत भी छिपी नहीं। वे जब गुजरात के समाज की बात करते हैं, तब धार्मिक प्रवृत्ति के हिस्से (टुकड़े) नहीं करते। सामाजिक परिवर्तन के लिए गैरसांप्रदायिक दृष्टि यहां बुनियादी शर्त है। धर्म और अध्यात्म, यह व्यक्ति की निजी उपासना का विषय है। सामाजिक कंकाल को आर्थिक शक्तियां सतत प्रभावित करती हैं। इसलिए धर्म को अलग रखकर परिस्थितिजन्य दबाव सर्जित करने पड़ेंगे। उसमें शब्द का भी यत्किंचित हिस्सा हो सकता है। इस संन्दर्भ में ‘व्यथा की बात’ का स्वागत होना चाहिए।
सन् 1989 में इन्हें उपन्यास ‘आंगलियात’ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें दलित पुरुषों का अन्याय के विरुद्ध प्रतिकार, प्रेमियों का संयम, वर्ग-संघर्ष और दूसरों के लिए कुछ करने की भावना दृश्यात्मक घटनाओं द्वारा व्यक्त हुई है। खेड़ा जिला के हरिजन-ईसाइयों की बोलचाल की भाषा को योग्य बनाकर जोसफ ने एक नई ताकत पैदा की है। इस अर्थ में वे पूर्व पीढ़ी के उसी विस्तार के ईश्वर पेटलीकर की तुलना में अधिक महत्त्वपूर्ण हैं। सो हरिजनों-दलितों के आर्थिक-जातीय शोषण के प्रति पेटलीकर द्वारा दिखाई सहानुभूति के वे ऋणी है। नौवें दशक का उपन्यास पेटलीकर के उत्तराधिकारी की राह देखता था। जोसफ को मिली प्रतिष्ठा हमारे साहित्य के इतिहास की आवश्यकता थी।
संभव है, कलावादी धीरे-धीरे जोसफ से विमुख होते जाएं। क्योंकि लोकप्रियता जिस सरलता की अपेक्षा रखती है, वह बहुतेरे कलाविदों को चुभती है।
शायद ‘व्यथा की बात’ जोसफ के सर्जक व्यक्तित्व का मुख्य तत्त्व है। एक परिचित सृष्टि उनकी अपनी आबोहवा के साथ इस पुस्तक द्वारा सुलभ होती है।
जोसफ के भाषा-प्रभुत्व की मुख्य पद्घति यहां चमत्कृति का अनुभव कराती है। ‘आंगलियात’ में इसी शक्ति का उदय है। ‘व्यथा की बात’ के रेखांचित्र उपन्यास पढ़ने का आनंद देने के साथ भावुक पाठक की सामाजिक संप्रज्ञता भी बढ़ाते हैं। प्रश्न उठता है-मैं जिस गुजरात में रहता हूं उसे कितना पहचानता हूं ?
‘व्यथा की बात’ की रचनाएं मात्र रेखाचित्र हैं या उनमें उपन्यास की कला भी है ? लेखक को क्या सिद्ध करना है ?
‘व्यथा की बात’ के रेखाचित्र साहित्य की श्रेणी में आते हैं, इसका मुख्य कारण रशियन कथा-लेखक की तरह जोसफ के अनुभवों की पूंजी है, उनके द्वारा व्यक्त हुई समूह चेतना है। यहां तक आते-आते वे साहित्य में प्रयुक्त होते जाते बोलचाल के शब्दों की ध्वनि से परिचित हो चुके थे। यह पुस्तक प्रकाशित हुई तब उन्होंने पचासवें में प्रवेश कर लिया था, इसलिए रंगदर्शिता को शांत हृदय से नाथने की प्रौढ़ता उनमें आ चुकी थी। संग्रह लेकिन समस्त रेखाचित्रों में से किसी को कमतर कहने की गुंजाइश नहीं है। संग्रह के जिसमें अनोखापन अधिक हो, वैसा एक रेखाचित्र है ‘हेझल पद्मणी’। यह रेखा-चित्र स्वातंत्र्योत्तर कहानियों के संपादन में भी समाविष्ट हो सकता है। संतति की तीव्र लालसा और लोक-संस्कृति की नैतिकता के दो भिन्न परिबल इस कृति में एक मनोघटना सृजित करते हैं। बाह्य परिस्थिति की प्रतीतिजनक वास्तविकता उसमें सहायक बनती है।
‘हेझल का पति’ रुड़ा हज्जाम’ बाहर से आकर पंचों की स्वीकृति से इस गांव का निवासी बनता है। मुख्यरूप से बुनकरों का। पंचायत के प्रमुख अंधे मेठा ने कहा, ‘‘चमार हमारी तरफ, लेकिन भंगी अलग, उन्हें नहीं छूना होगा।’’
रुड़ा को साल के बारह रुपए किराए पर मिलता है। नीम के नीचे बैठकर वह सबसे बातें करता है। लेखक ने पहले की तरह ‘दो बाघ मिल जाएं’ वैसी देह और लड़कों की नजर में ‘कादू मकराणी’ कहकर उसकी शरीर संपदा का वर्णन किया था उसी तरह उसकी हज्जाम के रूप में उसकी कला को स्वीकार किया है :
‘‘रुड़ा का हाथ जितना हल्का था उतना ही रेशम जैसा था। सिर पर फिरता होता तो नींद के झोंके आते, चेहरे पर घूमता होता तो संगमरमर-सा चिकना लगता। जूं-लीख से भरे बालों वाले लड़कों का सिर अपनी टांग और जांघ से दबाकर सिर मूंड़ देता।’’ तीसरे झण फिर गंजा, सफाचट और फिर दूसरे लड़के चिढ़ाते, ‘बोडी तकोडी माथामां जींगोडी, बावो बोलावे तुंतुं !’ एक उतनी ही देर रुड़ा बुरा दिखता, बाकी वह सबको खूब अच्छा लगता।
यह वर्णन कल्पना से नहीं हो सकता, सूक्ष्म निरीक्षण चाहिए, जो जोसफ, मकवान ने बचपन में अनायास किया है। पति का पात्र निरुपित कर, उसके सौम्य लेकिन विषय व्यक्तित्व का निर्देश कर लेखक उसकी पत्नी का परिचय कराता है, ‘‘एक भरी दोपहरी में वह वापस आया तो हाथ भर का घूंघट निकाले एक नाजुक स्त्री, सेर-सेर भर के पायल झनकारती उसके पीछे चल रही थी। उसी शाम पंचों के आगे उस स्त्री ने आंचल फैलाया और सवा रुपए से उसकी गोद भरकर गांववालों ने नाई की पत्नी को अपना लिया। परछन करने वाली स्त्रियों ने बताया कि रुड़ा की पत्नी है तो रूप का टुकड़ा। हाल ही में स्वांग दिखाने वाले ‘होथल पद्मणि’ का नाटक दिखा गए थे। होथल गांव के लोगों की जबान पर चढ़ गई और अपने सुंदर रूप के कारण हेझल पद्मणि बन गई।’’
रुड़ा और हेझल का संसार अब दो परिप्रेक्ष्य में निरूपित होता है। हेझल के रूप में प्रभावित हुए लोगों के व्यवहार का आकर्षक शैली में आलेखन होता है तो स्वमानी और शीतवंती हेझल पति के पुत्र न होने की पीड़ा व्यक्त करती रहती है। एक बार उसकी बेसब्री बढ़ जाती है।
‘ऊपरवाला सब अच्छा करेगा।’ पति का यह अश्वासन भी उसे धैर्य नहीं बंधा पाता तब रुड़ा उसकी विशेषता के संबंध में एक बात कहता है। जैसे उसके विवाह गीतों की प्रशंसा होती, उसी तरह उसके कंठ से गाए जाते मरसिया (शोक गीत) से एक शोकाकुल वातावरण सृजित होता। लेकिन रुड़ा कहता है, ‘‘तुम्हारे गले से आवाज निकलती है और मेरे अंग गलने-पिघलने लगते हैं।...भले जो हो आकाश भी फटे, तो भी तुम्हें मरसिया तो नहीं ही गाना है। तुम्हारी मां....’’
हेझल की मां ने मारमल्ल दादा के सात मरसिया माने थे। वह जीते जी उसमें से पांच पूरे कर चुकी थी। बाकी रहे दो हेझल को गाने थे। मां की मृत्यु के समय की बात वह नहीं तोड़े। काफी गानेवालियों का सौभाग्य रहा है और घर-घर झूले (बच्चों के) बंधे हैं।
और रुड़ा गुस्से से जूता मारता है। कलाई उतर जाती है। सौभाग्य की सूचक चूड़ियों की जोड़ टूट जाती है...उस दिन उसने पति की बात का उल्लंघन करने का निश्चय किया था...लेकिन वह दूसरे गांव गया था तब हेझल की सहेली रतन के जवान पति की मृत्यु हो जाती है। बाहर से आई मरसिया गाने वाली ‘रुदाली’ नहीं है। इसलिए हेझल को बुलाया जाता है। पति की अरुचि हेझल को याद है। वह मना करती है। बात वहीं पूरी नहीं होती। पंचों की तरफ से अंधे मेठा का हुक्म होता है, ‘‘या तो गाओ या गांव, शहर और यह परगना छोड़कर जहां चाहो, चली जाओ।’’
यहां चलचित्र ‘रुदाली’ का स्मरण होता है। दूसरों की तरफ से शोक-गीत गाना, यही उनकी जीविका का आधार होता है।
कितने की विवेचक दलित साहित्य को सपाट और प्रचारात्मक कहकर उसकी निंदा करते हैं। यहां लौकिक वास्तविकता के साथ आधिभौतिक परिबलों, उन परिबलों के विषय में रुढ़ मान्यताओं, वृत्तियों और फिर उन्हें बदलने की वृत्ति-इन सबका कैसा संकुल आलेखन हुआ है !
रतन पंचों के आगे आंचल फैलाकर हेझल को गांव छोड़ने से बचाने का प्रयत्न करती, उससे पहले ही हेझल मरसिया गाने लगती है।
लेखक ने मरसिया तथा झंपताल के साथ पूरा होता मरसिया भी प्रस्तुत किया है। लेखक को इसकी मात्र जानकारी ही नहीं, वह स्वयं इससे वाकिफ भी है।
रतन की चूड़ियां तोड़ते-तोड़ते ही हेझल को मूर्छा आ जाती है।
पहले पति के साथ सम्मत न हुई हेझल अब ऐसी ग्रंथि से पीड़ित है कि पति की बात का उल्लंघन करने का पाप उसके लिए रुकावट बन गया। मां बनने के उसके अरमान अधूरे रह गए।
रतन डाक्टर की बात करती है। रुड़ा नकारता नहीं है, लेकिन डाक्टर के यहां साथ जाने के लिए राजी नहीं होता। हेझल के अंतिम मरसिया गाने के बाद से दोनों के बीच जैसे अंतर बढ़ जाता है। रतन के साथ हेझल अस्पताल जाती है, तब जवान डाक्टर हेझल को देखकर जैसे विस्मित-सा रह जाता है। स्वस्थ काया और तीन दशक का निखरा रूप ! ‘यही है हेझल ! कुछ समय पहले जिसने मरसिया गाया था ? डाक्टर उसका दर्द भूलकर उसकी देह को ही जैसे पढ़ने लगा था।’
दलित नारी के दर्द के इलाज के बहाने उसका जातीय शोषण कैसी चतुरता से होता है, इसका आलेखन बाद में हुआ है। कुछ मुलाकातों के बाद डाक्टर, हेझल के साथ छूट पा लेता है। हेझल जैसे सर्वस्व खो देती है। ‘ओरिजनल सीन’ की ईसाई ग्रंथि और भारत के ग्रामीण श्रमजीवी की नैतिक समानता यहां समझदारीपूर्वक हेझल के व्यवहार में व्यक्त होती है। रतन उसे समझाने का प्रयत्न करती तो वह कहती है, ‘‘मेरा भाग्य खराब, मेरा पेट कुपात्र, मेरा गला कुपात्र और मेरा जीवन भी कुपात्र। जीने की कोई इच्छा अब नहीं रही मुझे !’’
हेझल सूखती जाती है और एक सुबह कहीं चली जाती है। ढूंढ़ने गया रुड़ा एक महीने बाद वापस आता है। वह भले ही कहता है कि ‘हेझल मायके में है’, लेकिन उसकी ढीली आवाज हेझल के जिंदा होने का विश्वास नहीं दिलाती।
कथा के प्रारंभ का रुड़ा और हेझल कैसे-कैसे स्थित्यंतरों से गुजर कर कहां से कहां पहुंचते हैं। जिन परिबलों के कारण जहां उन्हें झेलने की स्थिति आती है, वहीं वाचाल बनकर ध्यान खींचना नहीं आता। लेकिन कृति का पहला वाक्य ‘दो बाध जितनी देह’ रुड़ा और हेझल दोनों के संदर्भ में अर्थ समर्पक फैसला है। अंत में जो संवेदना जागती है, वही मरसिया का धुंधला रुप धारण कर लेती है। हेझल चली गई है, उस दिशा में से कोई अरूप रुपाली गा रही है।
दलित समाज के दुख इतने अधिक हैं कि उनका यथावत् प्रतिबिंब शब्दस्थ किया जाए तो भी उसमें अतिशयोक्ति लगेगी। कभी कथा साहित्य की घटनाओं की अपेक्षा हकीकत, अधिक आश्चर्यजनक लगती हो, ऐसा लगता है। ‘घर का दीया’ में मेलोड्रामा-अतिरंजन का तत्व लगता है। लेकिन लेखक को तो तथ्य ही पेश करना था। सास विधवा हो और बहू भी विधवा हो जाए यह परिस्थिति एक दलित परिवार के लिए दुखों के हिसाब की अपेक्षा दुखों के गुणाकार जैसी है। पुत्र मरा तब बहू सगर्भा थी। बेटे को साथ लेकर मजदूरी पर जाती बहू, चेतन उड़ जाने के बाद भी मजदूरी करना चालू रखती है और मजदूरी का रुपया मिलने पर घर आती है। पहले वह रुपया आशी मां (सास) के हाथ में देती है और फिर ? ‘और यह आपके घर का दीया !’ मां और दादी मां के रुदन को अव्यक्त रखकर लेखक ने घुटन का अद्भुत अनुभव कराया है। मृत्यु यहां कैसे विविध रूप में आती है ! जिसने बारह वर्ष से बनवास लिया है उस ‘भवान भगत’ का जवानजोध लड़का मर गया है, यह समाचार सुनकर भवान भगत आकाश की तरफ नजर डालकर कहते हैं, ‘‘तुम मुझे चैन से मरने दोगे, ऐसा नहीं लगता !’’ जीवन भर की श्रद्धा विचलित कर देने वाली समझदार-से-समझदार आदमी को भी मूढ़ बना देने वाली मृत्यु ‘व्यथा की बात’ को मितभाषी बनाती है। हृदय-विदारक रुदन के सामने बाधक मौन उत्पन्न कर जोसफ मकवान ने सूक्ष्म कलासूत्र दर्शाया है।
यह पुस्तक गुजराती साहित्य के विद्यार्थियों ने पाठ्यपुस्तक के रूप में पढ़ी है। नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा भारत की विभिन्न भाषाओं में अनुवाद के लिए इसका चुनाव पाठकों को साहित्य का आस्वाद कराने के साथ ग्रामीण भारत के विशाल उपेक्षित श्रमजीवी वर्ग की पहचान भी देगी। यह पहचान परिवर्तन का इष्ट संकेत बन सकेगा।
-रघुवीर चौधरी
1
थीं, तब मेरी तीन-तीन मांएं थीं !
मैं बिना मां के बेटा हूं। थीं, तब मेरी तीन-तीन मां थीं। चार से लेकर चौदह वर्ष की आयु तक प्यार-दुलार से उन्होंने मेरी जिंदगी में रंग भरे-ममता के, मानवता के, मातृत्व के ! और इच्छा बढ़ती जाए, ऐसा आघात देकर वह चली गई। पीछे छोड़ती गई मां नाम की वस्तु की एक ऐसी अदम्य भूख अभिशाप बनकर मेरी जिंदगी को आज भी पीड़ा दे रही है।
बालक को स्तनपान कराती मोह-समाधि में डूबी किसी मां को देखता हूं तो आज भी मेरा हृदय भावनाओं में खो जाता है। घरबार छोड़कर जाती स्त्री की भूल कभी मेरे मन में नहीं रही, और जिंदगी जड़मूल से उखाड़ देती स्त्री की विवशता तो मेरी भावनाओं पर पक्षघात कर देती है।
भाव से भरे ‘मां’ शब्द के जवाब में भरे हृदय से ‘बेटा’ ‘पुत्र’ का उद्गार सुनता हूं तो स्वर्ग मुझे एकदम नजदीक लगता है। एक बार दसवीं कक्षा में सुभद्रा जी की ‘मेरा बचपन’ कविता पढ़ाते समय गला भर आया। आंखें गीली हो गई। कक्षा के विद्यार्थी स्तब्ध रह गए। एक-दो को हंसी भी आई मैंने देखा-एक छात्र की आंख में आंसू थे। क्लास समाप्त हो, इस प्रतीक्षा में पांच मिनट हम मौन रहे। दर्द से प्रभावित वह दुर्गम समय एक युग की वेदना में डुबो गया। बाहर निकलकर चार कदम बढ़ा था कि आवाज आई, ‘‘सर !’’
पीछे देखा । वही रो रहा विद्यार्थी।
‘‘मेरी भी मां नहीं !’’ गहरी सहानुभूति प्रकट कर वह सीढ़ियां उतर गया। इस संसार में हम दो समान दुखिया थे। बिना ‘मां’ के, मां के प्रेम से, मां की छाया से वंचित।
छह वर्ष की आयु में मैंने मां को खोया था। अपनी यादाश्त पर कभी स्वयं मुझे आश्चर्य होता, वह इतनी प्रभावशाली थी। मेरे बचपन की अनेक यादें वैसी-की-वैसी ही आज भी मेरी स्मृति-भंडार में सुरक्षित रही हैं। मेरी ‘मां’ का चेहरा आज भी मेरी स्मृति में हू-ब-हू स्थिर है। मैं यदि चित्रकार होता, तो उसका रेखा-चित्र बना सकता था, ऐसा रेखा-चित्र कि एक भी रेखा न चूकता ! मां गुणवती थी, अनेक के मुंह से सुना है। सुंदर थी, स्नेहमयी थी। नाम था उसका हीरी। मेरी दादी और बुआ उसे ‘हीरा’ कहतीं। उसके गुणग्राहक कहते कि घर की राह वह ‘हीरा’ ही थी।
उसे टी.बी था। पुराने सिविल अस्पताल में उसे उपचार के लिए दाखिल किया था। वहां से मेरे पिता को लिखा उसका एक पत्र संदूक में मिला था। पेंसिल से घुमावदार अक्षरों में उसने एक-एक बात लिखी थी। पिताजी ईसाई स्कूल में शिक्षक थे। खंभोलज गांव में रहते थे। घर के पीछे विशाल अहाता था। उस पत्र में, जिस तरह मुर्गी अंडे सेती हैं, उसी तरह मां ने अहाते में भिंडी और सेम बोने की और उसकी देखभाल करने की इच्छा व्यक्त की थी। हमारे लिए तो यह चिंता की बात थी ही, लेकिन लड़की के संदूक में एक तरफ रखी शीशी घर पहुंचाने तथा हर रविवार को हमें चाय के साथ दो-दो चम्मच रेंड़ी का तेल पिलाने की खास सूचना भी मेरी चाची को देना नहीं भूली थी।
मां के हम दो बेटे। बड़ा भाई मनु और उससे छह वर्ष छोटा मैं। बीच में एक बहन का जन्म हुआ था, लेकिन वह अधिक समय जीवित नहीं रही। मां की बीमारी के बीच हमें हमारे गांव ‘ओड’ में हमारी दादी धनीबा के पास छोड़ दिया गया। दादी के यहां पांच-छह गाय-भैंसें थीं। दूध-घी की कोई कमी नहीं थी। पहलवान जैसे उनके बेटे-बहू निस्संतान थे, इसलिए वे दोनों हमें बहुत स्नेह करते।
मां की बीमारी के बीत ही पिताजी का एक दूसरी महिला के साथ संबंध जुड़ गया था। कुछ स्वस्थ होकर मां अस्पताल से घर आई तो उसे इस बात का पता चला। उसे चोट पहुंची। लोग बताते हैं-हीरा जीवित रहती, लेकिन यह बात जानने के बाद जिंदा रहने में उसकी रुचि न रही।
हमारी ‘नई मां’ बनकर वह महिला आई। वह घटना आज भी यथावत याद है।
दादी ने पिताजी से कहा था, ‘‘यदि तुम उसे इस घर में लाआगे तो मेरा मरा मुंह देखोगे !’’
छोटे चाचा शिक्षित थे। पिताजी की हर बात मान लेते थे, लेकिन वे भी नाराज थे। पिताजी एक बार जो तय कर लेते थे वह तय ही होता था। ठीक बरात जाने के दिन ही दादी ने आंखें मूंद लीं। तीन बजे मेरी मां की कब्र के पास ही दादी की कब्र खोदी गई और उसमें दादी को दफनाकर लौटने के बाद कुछ देर सब आंगन में बैठे। उसके आधे घंटे बाद ही पिताजी की बारात चली। हमें भी बारात में शामिल किया गया। मेरे बड़े भाई ने न चलने का हठ किया, उसे बुआ ने रोते-रोते समझाया। मैं तो जाने की हठ कर रहा था। चाचा नहीं गए। दूसरे दिन सुबह बारात लौटी। चार कोस का रास्ता पैदल चलना था। कोई मुझे गोद में उठा लेता, कोई उंगली पकड़कर चलता। बीच में दो कोस की गोचर भूमि थी। उस गोचर भूमि में ही मेरी किसी ने मेरी नयी मां को सुनाकर कहा, ‘‘जाओ, तुम्हारी मां तुम्हें गोद में उठा लेगी।’’ और चुपचाप चल रही नई मां को यह सुनकर जैसे ख्याल आया, ‘‘आओ बेटा, मैं उठा लेती हूं।’’ कहते हुए उसने मुझे बुलाया और लपककर मैं उसकी गोद में चढ़ता उससे पहले ही मेरा बड़ा भाई मनु बोल उठा,....‘‘जास्या... नहीं जाना ! देखो, इसी जगह हमारी मां को दफनाया गया है।’’
और मेरी स्मृति में चुभन होने लगी। अस्पताल से मां के वापस आने के बाद इसी रास्ते से हम ‘ओड’ गांव जा रहे थे। हम दोनों भाई खेलते-कूदते धीरे-धीरे चल रहे थे और मां गोद में उठाने की बात को लेकर पिताजी से झगड़ रही थी। गुस्से में पिताजी ने मां को छाते से इतना मारा कि वह धरती पर गिर पड़ी। आवेश में आकर मारा था। मां को खांसी शुरू हुई और खून की उल्टी। बिना कुछ परवाह किए पिताजी आगे बढ़ गए थे। इस निर्जन गोचर भूमि में मां से लिपटकर हम दोनों भाई जोर से रो पड़े थे। हम दोनों को छाती से लगाकर मां अपने आहत अपमान से जितना नहीं, उतना हमारे भविष्य की कल्पना से सिसक-सिसककर रो पड़ी थी। संयोग से यह वही जगह थी। भाई की आवाज ने मेरे ज्ञानतंतु को जगा दिया और नई मां की गोद को झटका देकर मैं भाई के पास पहुंच गया। पिताजी की आंखों से अंगारों की वर्षा हो रही थी, लेकिन भाई तो भीगी आंखों से वह जगह ही देख रहा था। उस जगह ने मेरी मां का स्थान मेरे हृदय के किसी कोने में ऐसा तो जड़ दिया था कि पूरे रौब से पिताजी ने हमें नई मां को ‘मां’ कहने को कहा, फिर भी अपनी ‘मां’ का वह स्थान हृदय से नहीं हटा तो नहीं ही हटा और नया संबोधन प्रतिष्ठित नहीं हो सका। जीवनभर नहीं हो सका।
उस गोचर भूमि से उस दिन से पीड़ित मां के साथ घर लौटने के बाद मां तो मौन ही रही, लेकिन मैंने तथा बड़े भाई ने दादी से वे सारी बातें बता दीं। उसने अपने बेटे की खबर ली। मां रोती-रोती मेरी दादी तथा छोटी चाची के आगे आंचल फैला कर गिड़गिड़ा रही थी। भाई ने मुझे समझाया कि हमारी मां मरने से पहले से ही हमें दूसरों को सौंपती रही है। लेकिन तब हमने मौत को देखा-समझा नहीं था।
इस घटना के बाद मां ने बिस्तर पकड़ लिया। छोटी चाची और बुआ उसकी सेवा खड़े पांव करती थीं। मां हमें अपने बिस्तर के पास अधिक देर ठहरने नहीं देती थी। उसकी सांस के कीटाणु हमारे जीवन में प्रवेश न करें, इस बात की उसे चिंता होती। बहुत बार अपने पायताने हमें खड़ा रखकर वह टकटकी बांधकर हमें निहारती रहती और उस समय उसकी आंखों से चौधार आंसू बहते रहते। बुआ उसके आंसू पोंछती और रोती-रोती हमें बाहर खेलने के लिए भेज देती। ऐसे समय बड़ा भाई असहाय हो जाता। पुस्तक ले वह ओसारे के पीछे वाले कमरे में चला जाता मां से उसकी सिसकियां सहन न होतीं। वह जबर्दस्ती हंसने का प्रयत्न करती और मेरे बड़े भाई मनु से अपनी कविता सुनाने को कहती।
मैं बिना मां के बेटा हूं। थीं, तब मेरी तीन-तीन मां थीं। चार से लेकर चौदह वर्ष की आयु तक प्यार-दुलार से उन्होंने मेरी जिंदगी में रंग भरे-ममता के, मानवता के, मातृत्व के ! और इच्छा बढ़ती जाए, ऐसा आघात देकर वह चली गई। पीछे छोड़ती गई मां नाम की वस्तु की एक ऐसी अदम्य भूख अभिशाप बनकर मेरी जिंदगी को आज भी पीड़ा दे रही है।
बालक को स्तनपान कराती मोह-समाधि में डूबी किसी मां को देखता हूं तो आज भी मेरा हृदय भावनाओं में खो जाता है। घरबार छोड़कर जाती स्त्री की भूल कभी मेरे मन में नहीं रही, और जिंदगी जड़मूल से उखाड़ देती स्त्री की विवशता तो मेरी भावनाओं पर पक्षघात कर देती है।
भाव से भरे ‘मां’ शब्द के जवाब में भरे हृदय से ‘बेटा’ ‘पुत्र’ का उद्गार सुनता हूं तो स्वर्ग मुझे एकदम नजदीक लगता है। एक बार दसवीं कक्षा में सुभद्रा जी की ‘मेरा बचपन’ कविता पढ़ाते समय गला भर आया। आंखें गीली हो गई। कक्षा के विद्यार्थी स्तब्ध रह गए। एक-दो को हंसी भी आई मैंने देखा-एक छात्र की आंख में आंसू थे। क्लास समाप्त हो, इस प्रतीक्षा में पांच मिनट हम मौन रहे। दर्द से प्रभावित वह दुर्गम समय एक युग की वेदना में डुबो गया। बाहर निकलकर चार कदम बढ़ा था कि आवाज आई, ‘‘सर !’’
पीछे देखा । वही रो रहा विद्यार्थी।
‘‘मेरी भी मां नहीं !’’ गहरी सहानुभूति प्रकट कर वह सीढ़ियां उतर गया। इस संसार में हम दो समान दुखिया थे। बिना ‘मां’ के, मां के प्रेम से, मां की छाया से वंचित।
छह वर्ष की आयु में मैंने मां को खोया था। अपनी यादाश्त पर कभी स्वयं मुझे आश्चर्य होता, वह इतनी प्रभावशाली थी। मेरे बचपन की अनेक यादें वैसी-की-वैसी ही आज भी मेरी स्मृति-भंडार में सुरक्षित रही हैं। मेरी ‘मां’ का चेहरा आज भी मेरी स्मृति में हू-ब-हू स्थिर है। मैं यदि चित्रकार होता, तो उसका रेखा-चित्र बना सकता था, ऐसा रेखा-चित्र कि एक भी रेखा न चूकता ! मां गुणवती थी, अनेक के मुंह से सुना है। सुंदर थी, स्नेहमयी थी। नाम था उसका हीरी। मेरी दादी और बुआ उसे ‘हीरा’ कहतीं। उसके गुणग्राहक कहते कि घर की राह वह ‘हीरा’ ही थी।
उसे टी.बी था। पुराने सिविल अस्पताल में उसे उपचार के लिए दाखिल किया था। वहां से मेरे पिता को लिखा उसका एक पत्र संदूक में मिला था। पेंसिल से घुमावदार अक्षरों में उसने एक-एक बात लिखी थी। पिताजी ईसाई स्कूल में शिक्षक थे। खंभोलज गांव में रहते थे। घर के पीछे विशाल अहाता था। उस पत्र में, जिस तरह मुर्गी अंडे सेती हैं, उसी तरह मां ने अहाते में भिंडी और सेम बोने की और उसकी देखभाल करने की इच्छा व्यक्त की थी। हमारे लिए तो यह चिंता की बात थी ही, लेकिन लड़की के संदूक में एक तरफ रखी शीशी घर पहुंचाने तथा हर रविवार को हमें चाय के साथ दो-दो चम्मच रेंड़ी का तेल पिलाने की खास सूचना भी मेरी चाची को देना नहीं भूली थी।
मां के हम दो बेटे। बड़ा भाई मनु और उससे छह वर्ष छोटा मैं। बीच में एक बहन का जन्म हुआ था, लेकिन वह अधिक समय जीवित नहीं रही। मां की बीमारी के बीच हमें हमारे गांव ‘ओड’ में हमारी दादी धनीबा के पास छोड़ दिया गया। दादी के यहां पांच-छह गाय-भैंसें थीं। दूध-घी की कोई कमी नहीं थी। पहलवान जैसे उनके बेटे-बहू निस्संतान थे, इसलिए वे दोनों हमें बहुत स्नेह करते।
मां की बीमारी के बीत ही पिताजी का एक दूसरी महिला के साथ संबंध जुड़ गया था। कुछ स्वस्थ होकर मां अस्पताल से घर आई तो उसे इस बात का पता चला। उसे चोट पहुंची। लोग बताते हैं-हीरा जीवित रहती, लेकिन यह बात जानने के बाद जिंदा रहने में उसकी रुचि न रही।
हमारी ‘नई मां’ बनकर वह महिला आई। वह घटना आज भी यथावत याद है।
दादी ने पिताजी से कहा था, ‘‘यदि तुम उसे इस घर में लाआगे तो मेरा मरा मुंह देखोगे !’’
छोटे चाचा शिक्षित थे। पिताजी की हर बात मान लेते थे, लेकिन वे भी नाराज थे। पिताजी एक बार जो तय कर लेते थे वह तय ही होता था। ठीक बरात जाने के दिन ही दादी ने आंखें मूंद लीं। तीन बजे मेरी मां की कब्र के पास ही दादी की कब्र खोदी गई और उसमें दादी को दफनाकर लौटने के बाद कुछ देर सब आंगन में बैठे। उसके आधे घंटे बाद ही पिताजी की बारात चली। हमें भी बारात में शामिल किया गया। मेरे बड़े भाई ने न चलने का हठ किया, उसे बुआ ने रोते-रोते समझाया। मैं तो जाने की हठ कर रहा था। चाचा नहीं गए। दूसरे दिन सुबह बारात लौटी। चार कोस का रास्ता पैदल चलना था। कोई मुझे गोद में उठा लेता, कोई उंगली पकड़कर चलता। बीच में दो कोस की गोचर भूमि थी। उस गोचर भूमि में ही मेरी किसी ने मेरी नयी मां को सुनाकर कहा, ‘‘जाओ, तुम्हारी मां तुम्हें गोद में उठा लेगी।’’ और चुपचाप चल रही नई मां को यह सुनकर जैसे ख्याल आया, ‘‘आओ बेटा, मैं उठा लेती हूं।’’ कहते हुए उसने मुझे बुलाया और लपककर मैं उसकी गोद में चढ़ता उससे पहले ही मेरा बड़ा भाई मनु बोल उठा,....‘‘जास्या... नहीं जाना ! देखो, इसी जगह हमारी मां को दफनाया गया है।’’
और मेरी स्मृति में चुभन होने लगी। अस्पताल से मां के वापस आने के बाद इसी रास्ते से हम ‘ओड’ गांव जा रहे थे। हम दोनों भाई खेलते-कूदते धीरे-धीरे चल रहे थे और मां गोद में उठाने की बात को लेकर पिताजी से झगड़ रही थी। गुस्से में पिताजी ने मां को छाते से इतना मारा कि वह धरती पर गिर पड़ी। आवेश में आकर मारा था। मां को खांसी शुरू हुई और खून की उल्टी। बिना कुछ परवाह किए पिताजी आगे बढ़ गए थे। इस निर्जन गोचर भूमि में मां से लिपटकर हम दोनों भाई जोर से रो पड़े थे। हम दोनों को छाती से लगाकर मां अपने आहत अपमान से जितना नहीं, उतना हमारे भविष्य की कल्पना से सिसक-सिसककर रो पड़ी थी। संयोग से यह वही जगह थी। भाई की आवाज ने मेरे ज्ञानतंतु को जगा दिया और नई मां की गोद को झटका देकर मैं भाई के पास पहुंच गया। पिताजी की आंखों से अंगारों की वर्षा हो रही थी, लेकिन भाई तो भीगी आंखों से वह जगह ही देख रहा था। उस जगह ने मेरी मां का स्थान मेरे हृदय के किसी कोने में ऐसा तो जड़ दिया था कि पूरे रौब से पिताजी ने हमें नई मां को ‘मां’ कहने को कहा, फिर भी अपनी ‘मां’ का वह स्थान हृदय से नहीं हटा तो नहीं ही हटा और नया संबोधन प्रतिष्ठित नहीं हो सका। जीवनभर नहीं हो सका।
उस गोचर भूमि से उस दिन से पीड़ित मां के साथ घर लौटने के बाद मां तो मौन ही रही, लेकिन मैंने तथा बड़े भाई ने दादी से वे सारी बातें बता दीं। उसने अपने बेटे की खबर ली। मां रोती-रोती मेरी दादी तथा छोटी चाची के आगे आंचल फैला कर गिड़गिड़ा रही थी। भाई ने मुझे समझाया कि हमारी मां मरने से पहले से ही हमें दूसरों को सौंपती रही है। लेकिन तब हमने मौत को देखा-समझा नहीं था।
इस घटना के बाद मां ने बिस्तर पकड़ लिया। छोटी चाची और बुआ उसकी सेवा खड़े पांव करती थीं। मां हमें अपने बिस्तर के पास अधिक देर ठहरने नहीं देती थी। उसकी सांस के कीटाणु हमारे जीवन में प्रवेश न करें, इस बात की उसे चिंता होती। बहुत बार अपने पायताने हमें खड़ा रखकर वह टकटकी बांधकर हमें निहारती रहती और उस समय उसकी आंखों से चौधार आंसू बहते रहते। बुआ उसके आंसू पोंछती और रोती-रोती हमें बाहर खेलने के लिए भेज देती। ऐसे समय बड़ा भाई असहाय हो जाता। पुस्तक ले वह ओसारे के पीछे वाले कमरे में चला जाता मां से उसकी सिसकियां सहन न होतीं। वह जबर्दस्ती हंसने का प्रयत्न करती और मेरे बड़े भाई मनु से अपनी कविता सुनाने को कहती।
हम तो सूरज के छड़ीदार, हम तो प्रभात की पुकार,
सूरज आए सात घोड़े वाले अरुण रथ पर
आगे चलता छड़ी पुकारूं, प्रकाश गीता गाता।
सूरज आए सात घोड़े वाले अरुण रथ पर
आगे चलता छड़ी पुकारूं, प्रकाश गीता गाता।
और-
भंवरे को घूमने का लोभ, गुन-गुन-गुन करता वह
सांझ पड़े घर ना आए, भटका-भटका फिरता वह।
सांझ पड़े घर ना आए, भटका-भटका फिरता वह।
यह कविता वह गाता और उसकी गाई हुई यह कविता पूरी-की-पूरी मुझे याद हो गई
थी। मुझे पढ़ना नहीं आता था, तो भी कई बार भाई की पुस्तक लेकर वह पूरी
कविता मैं तो गाकर सुनाता। मुर्गे के चित्र के कारण मैं पुस्तक सीधी
पकड़ता था लेकिन भौरे वाली कविता में चित्र नहीं था इसलिए कभी पुस्तक सीधी
पकड़ता था लेकिन भौंरे वाली कविता में चित्र नहीं था इसलिए कभी पुस्तक
मुझे इतना अच्छा लगता कि मैं उससे लिपट पड़ता। वह मेरे मुंह को चूमने के
लिए अपनी श्वास की बाधा के कारण तड़प-तड़पकर रह जाती और उसके गले से सिसकी
निकल पड़ती। चाचा आकर मुझे दूर ले जाते तब रो-रोकर मेरे चाचा तब जड़ बन
जाते।
मां को अपनी अंतिम घड़ी का आभास हो गया था। चाचा पिताजी को बुलाने जा रहे थे तो उन्हें हठ करके रोका। उसकी इच्छा से चाची और बुआ ने उसे नहला कर नई साड़ी पहनाई। हम दोनों भाइयों को अपनी पसंद के कपड़े पहनवा कर आंखों के आगे खड़ा रखा। उस शाम अपने हाथों उसने हमें हलुआ खिलाया और स्वयं भी शांति से एकाध कौर खाया। हठ करके मैंने अपनी कढ़ाई वाली टोपी पहनी और ‘विलियम टेल’ के नाटक का वाल्टर बनकर मां को खुश करने के लिए उसका अभिनय किया। दादी, बुआ, काफी तथा दूसरे कितने ही लोग उस शाम मां के आसपास घिरे रहे। क्या हो रहा है, इसकी समझ मुझे नहीं थी इसलिए नए कपड़ों को देखता-देखता कब सो गया, इसका पता न चला और सुबह जागा तब पूरे घर में रोना-धोना चल रहा था।
खंभोलज से वापस आकर पिताजी खंभे का सहारा लिए मुंह नीचा किए बैठे थे। पहाड़ जैसे मेरे काका छोटे बच्चों की तरह आक्रंद कर रहे थे और मेरा बड़ा भाई बेहोश हो गया था। मां की मृत्यु का आघात अभी मेरे नासमझ हृदय के सही स्थान पर लगा नहीं था, इसलिए वह कढ़ाई की गई टोपी पहनकर मैं रो रही स्त्रियों के बीच सोई मां के पास पहुंचा। तब मैं क्या बोला था, यह तो याद नहीं, लेकिन मां का सिर बुआ को थमाकर हाहाकार करती भाभी ने मुझे उसकी छाती से लगा दिया। उसके हृदय की धड़कन मेरे कानों से होकर मेरे कलेजे को छू गई। उसकी अनुभूति आज भी मुझे होती रहती है। बिन मां के मेरे भविष्य की भयंकर कल्पना थीं, तब मेरी तीन-तीन मांएं थीं !
मां को अपनी अंतिम घड़ी का आभास हो गया था। चाचा पिताजी को बुलाने जा रहे थे तो उन्हें हठ करके रोका। उसकी इच्छा से चाची और बुआ ने उसे नहला कर नई साड़ी पहनाई। हम दोनों भाइयों को अपनी पसंद के कपड़े पहनवा कर आंखों के आगे खड़ा रखा। उस शाम अपने हाथों उसने हमें हलुआ खिलाया और स्वयं भी शांति से एकाध कौर खाया। हठ करके मैंने अपनी कढ़ाई वाली टोपी पहनी और ‘विलियम टेल’ के नाटक का वाल्टर बनकर मां को खुश करने के लिए उसका अभिनय किया। दादी, बुआ, काफी तथा दूसरे कितने ही लोग उस शाम मां के आसपास घिरे रहे। क्या हो रहा है, इसकी समझ मुझे नहीं थी इसलिए नए कपड़ों को देखता-देखता कब सो गया, इसका पता न चला और सुबह जागा तब पूरे घर में रोना-धोना चल रहा था।
खंभोलज से वापस आकर पिताजी खंभे का सहारा लिए मुंह नीचा किए बैठे थे। पहाड़ जैसे मेरे काका छोटे बच्चों की तरह आक्रंद कर रहे थे और मेरा बड़ा भाई बेहोश हो गया था। मां की मृत्यु का आघात अभी मेरे नासमझ हृदय के सही स्थान पर लगा नहीं था, इसलिए वह कढ़ाई की गई टोपी पहनकर मैं रो रही स्त्रियों के बीच सोई मां के पास पहुंचा। तब मैं क्या बोला था, यह तो याद नहीं, लेकिन मां का सिर बुआ को थमाकर हाहाकार करती भाभी ने मुझे उसकी छाती से लगा दिया। उसके हृदय की धड़कन मेरे कानों से होकर मेरे कलेजे को छू गई। उसकी अनुभूति आज भी मुझे होती रहती है। बिन मां के मेरे भविष्य की भयंकर कल्पना थीं, तब मेरी तीन-तीन मांएं थीं !
|
|||||
लोगों की राय
No reviews for this book